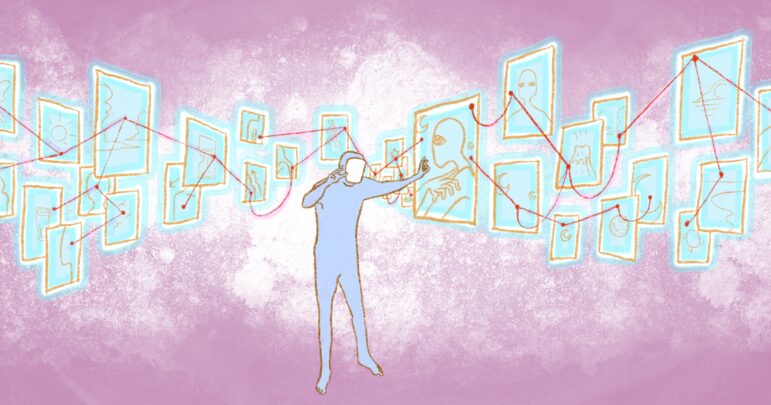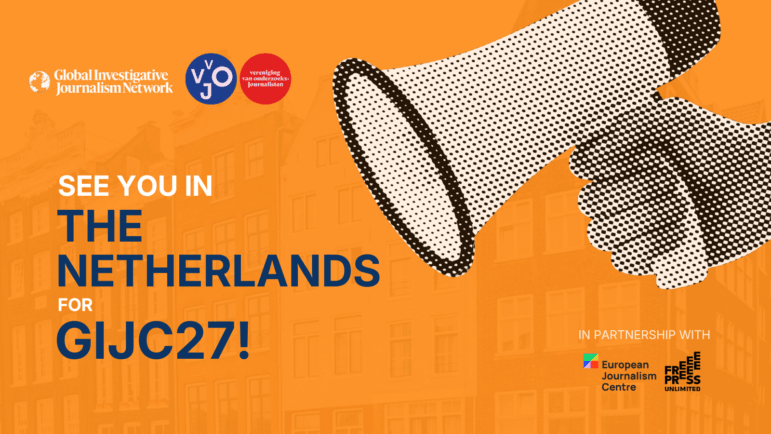Illustration: Siddhesh for GIJN
भारत को समझने के लिए जाति व्यवस्था को समझना जरूरी है। इसने 3000 से भी अधिक वर्षों तक जनता के अधिकारों का निर्धारण किया है। आज भी यह भारतीय समाज की नींव है। भारत के अलावा नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी यह प्राचीन व्यवस्था आज तक मौजूद है।
जाति एक वंशानुगत सामाजिक समूह है। किसी जाति के सदस्य पारंपरिक रूप से एक वंशानुगत व्यवसाय साझा करते हैं। वे एक ही पौराणिक पूर्वज का वंश का दावा करते हैं। वे लोग सामान्यत: अपने समुदाय के भीतर ही विवाह करते हैं। आम तौर पर समूह के बाहर सामाजिक मेलजोल भी न्यूनतम रखते हैं।
जातियाँ स्थिर नहीं रही हैं। उनका कई उपजातियों के रूप में विकास अथवा विभाजन हुआ है। लंबे समय के दौरान कुछ जातियों का अन्य जातियों में विलय भी देखने को मिला है। धर्मग्रंथों में धार्मिक स्वीकृति और जातिगत नियमों के निरंतर पालन के कारण हिंदुओं में सबसे अधिक जातियां देखने को मिलती हैं। भारत में सभी धर्मों में जाति है। हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में धर्मांतरित लोग अपनी सामाजिक प्रथाओं को भी अपने साथ उस धर्म में ले गए।
भारत की सामाजिक-आर्थिक गतिशीलता को समझना हो, तो जाति-व्यवस्था को समझें। समाज में मौजूद प्रणालीगत असमानताओं को दूर करने के लिए जातिगत मुद्दों की पड़ताल जरूरी है। किसी पत्रकार को रिपोर्टिंग के दौरान जाति व्यवस्था को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे आपको किसी व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसकी राजनीति, आर्थिक स्थिति और दृष्टिकोण को समझने में अंतर्दृष्टि मिल सकती है।
जाति व्यवस्था की जटिलताओं को समझने के लिए यह रिपोर्टिंग मार्गदर्शिका तैयार की गई है। इसमें आपको जाति-संबंधी मामलों की प्रभावी रिपोर्टिंग के लिए व्यावहारिक सलाह दी गई है। इसमें प्रस्तुत जानकारी भारत में काम करने वाले पत्रकारों के लिए खास उपयोगी है। साथ ही, यह उन देशों में कार्यरत पत्रकारों के लिए भी उपयोगी है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी रहते हैं। कारण स्पष्ट है। भारत के लोग जिन देशों में गए, वहां भी अपने साथ जाति व्यवस्था को ले गए हैं।
भारत में जातियां
विशाल और विविध भारत की आबादी 1.4 अरब से भी अधिक है। यहां क्षेत्र, भाषा और धर्म के अनुसार अलग-अलग जातिगत विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इससे उनकी समाजशास्त्रीय प्रकृति का पता चलता है। एक ही जाति के लोगों के खान-पान के तरीके अलग-अलग भौगोलिक इलाकों में अलग-अलग हो सकते हैं।
जातियों की संरचना पद-अनुक्रम के अनुसार होती है। प्रत्येक जाति के लिए सामाजिक व्यवस्था में एक निर्धारित स्थान है। ब्राह्मण को सबसे ऊपर माना जाता है। इस पद-अनुक्रम के अनुसार उस जाति के लोगों को सामाजिक लाभ मिलते हैं। जैसे, सत्ता तक पहुंच किस जाति के लोगों को होगी, यह जाति के अनुसार निर्धारित होता है। सामाजिक अनुक्रम में जो जाति जितनी नीचे होगी, सत्ता तक उसकी पहुंच उतनी ही कम होगी।
इसलिए जाति व्यवस्था एक सामाजिक-आर्थिक संकेतक के रूप में भी काम करती है। इसमें किसी जाति के लोगों की संपत्ति, भूमि स्वामित्व, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास तक उनकी पहुँच को देखा जा सकता है। जाति का निर्धारण केवल जन्म के आधार पर होता है। इसे बदला नहीं जा सकता।
- परंपरागत तौर पर ब्राह्मण जाति को ज्ञान का संरक्षक माना गया है। विद्यालयों, धर्मग्रंथों और देवताओं पर नियंत्रण होता है। उन्हें पुरोहित वर्ग माना जाता है।
- क्षत्रिय जाति को योद्धा वर्ग के बतौर देखा गया है। उनके पास हथियारों तक पहुंच थी। इस जाति के सदस्य सैनिक होते थे।
- वैश्य जाति लंबे समय से व्यापार से जुड़ी है। आज भी इस जाति के काफी सदस्य व्यापारी हैं।
- शूद्र को पारंपरिक रूप से किसान और कारीगर की श्रेणी में रखा गया है। उनकी भूमिका उक्त तीन जातियों की सेवा करना समझी जाती थी।
प्रत्येक जाति की हज़ारों उपजातियां भी हैं:
- अन्य पिछड़ा वर्ग और उपजातियाँ।
- अनुसूचित जातियां और उपजातियां।
- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य भी कई जातियों में विभाजित हैं। लेकिन भारत सरकार उनकी गणना नहीं करती। इसलिए उनके बारे में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है।
- भारतीय संविधान के निर्माता डॉ भीमराव रामजी अंबेडकर ने अपने निबंध, “जाति का अभिशाप” में ब्राह्मण जातियों का विवरण दिया था।

भारत के मदुरई स्थित एक मंदिर में अध्ययन करते युवा ब्राह्मण छात्र। ब्राह्मण जाति को भारत के विद्यालयों, धर्मग्रंथों और धर्म का संरक्षक माना जाता है। इमेज: शटरस्टॉक
चार वर्णों पर आधारित उक्त वर्गीकरण के अलावा हिंदुओं की एक पांचवीं या कथित अछूत श्रेणी भी है। इन्हें अन्य जातियों ने ‘अस्पृश्यता’ के नाम पर बहिष्कृत कर दिया था। इन्हें अब आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जाति के रूप में जाने जाता है। इस श्रेणी के लोग पारंपरिक रूप से कपड़े धोने, जूते बनाने, शराब बनाने, मजदूरी जैसी सेवा प्रदान करते थे। सवर्ण हिंदू उन्हें ‘अपवित्र’ मानते थे। अगर वे गलती से उन्हें छू लेते थे, तो शुद्धिकरण अनुष्ठान करते थे।
क्षेत्र के अनुसार, अस्पृश्यता का प्रचलन अलग-अलग था। कुछ जगहों पर, किसी कथित ‘अछूत’ को देखना भी अपशकुन माना जाता था। उन्हें सार्वजनिक कुओं से पानी भरने, हिंदू मंदिरों के समीप सड़कों पर चलने, अन्य हिंदुओं के साथ भोजन करने या स्कूलों में पढ़ने की अनुमति नहीं थी।
ब्रिटिश अधिकारियों ने अछूतों पर लगे कुछ प्रतिबंध हटा दिए। उन्होंने सभी भारतीयों के लिए सार्वजनिक कुएं खोल दिए। अछूत कहे जाने लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती किया। सबके लिए स्कूल खोल दिए। आजादी के बाद भारतीय संविधान ने उनके विरुद्ध भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। जाति व्यवस्था से बाहर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसके बावजूद भेदभाव जारी है।
स्वतंत्रता के बाद जाति प्रथा
अंग्रेजों के जाने के बाद 1950 में भारतीय संविधान ने जातिगत भेदभाव को गैरकानूनी घोषित कर दिया। अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया। जातिगत भेदभाव भारतीय समाज में काफी गहरे तक अंतर्निहित था। इसलिए संविधान ने हिंदू सामाजिक व्यवस्था में निचली जातियों को शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक सुरक्षा प्रदान की। ऐसा करके सभी नागरिकों के लिए अवसर समान उपलब्ध कराए गए। अछूत समझे जाने वाले समूहों को अनुसूचित जातियों के रूप में मान्यता दी गई। अनुसूचित जनजातियों को भी संविधान में संरक्षण दिया गया। उन्हें जनगणना में भी शामिल किया गया।
अन्य पिछड़ी जातियों (ओबीसी) को हिंदू वर्ण-व्यवस्था के भीतर निम्न सामाजिक स्तर पर रखा जाता था। माना जाता है कि निम्न सामाजिक स्तर ही उनके सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन का कारण है। लेकिन जनगणना में ओबीसी की गणना नहीं की जाती। ओबीसी की वास्तविक संख्या का पता लगाने का उच्च जाति के हिंदुओं द्वारा विरोध किया जाता रहा है। हिंदुओं में निचली जातियों का बहुमत है, इस बात को सवर्ण समाज स्वीकार नहीं करना चाहता। राजनीति, व्यवसाय और समाज में ओबीसी का आनुपातिक प्रतिनिधित्व नहीं है।
अब सकारात्मक कार्रवाई के उद्देश्य से भारतीय जनसंख्या का आधिकारिक वर्गीकरण किया गया है :
- सामान्य श्रेणी: इसमें सामाजिक रूप से विशेषाधिकार प्राप्त जातियां शामिल हैं- ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। शिक्षा और रोज़गार पर लंबे समय से इनका एकाधिकार रहा है। इसलिए संविधान इन जातियों को कोई विशेषाधिकार नहीं देता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) : इस श्रेणी में शूद्र शामिल हैं। 1980 में अंतिम गणना के दौरान इनमें जनसंख्या का 52 प्रतिशत शामिल था। सरकारी नौकरियों और शिक्षा में उन्हें 27 प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है। सरकारी कॉलेजों या विश्वविद्यालयों में प्रवेश के साथ ही शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों पर नियुक्ति में भी यह आरक्षण मिलता है। ओबीसी की पहचान में किसी जाति समूह की आर्थिक स्थिति को अप्रासंगिक माना जाता है। 1980 में हुई पिछली गणना के बाद से अब तक ओबीसी की वर्तमान जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। अंग्रेजों के बाद किसी भी सरकार ने कभी भी सभी जातियों की जनगणना नहीं कराई है। दक्षिणपंथी सत्तारूढ़ दल का दावा है कि जाति जनगणना हिंदुओं को विभाजित करने के लिए अंग्रेजों की साजिश थी। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 1980 में ओबीसी की अनुमानित जनसंख्या 52% निर्धारित की थी। उसकी रिपोर्ट 1991 में लागू की गई थी। पिछली जाति जनगणना के सौ साल बाद मोदी सरकार ने मई 2025 में घोषणा की है कि अगली जनगणना में जातियों की गणना की जाएगी।
- अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी। इसकी रिपोर्ट के अनुसार, अनुसूचित जाति (एससी) की जनसंख्या 16.6 प्रतिशत थी। इसमें वे लोग शामिल हैं, जो किसी भी जाति से संबंधित नहीं थे। यह सामाजिक रूप से हाशिए पर रह गए लोग हैं। इन्हें नौकरियों और शिक्षा में 15 प्रतिशत स्थान दिया जाता है। इसमें केवल हिंदू, सिख और बौद्ध शामिल हैं।
- अनुसूचित जनजाति (एसटी) आदिवासी या मूल निवासी हैं। यह समूह भी जाति व्यवस्था से बाहर है। इन्हें एनिमिस्ट माना जाता है, जो प्रकृति की पूजा करते हैं। इन्हें सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 7.5 प्रतिशत आरक्षण मिलता है।
एससी, ओबीसी और एसटी को संरक्षित संवैधानिक वर्ग के बतौर रखा गया है। ओबीसी और एसटी में क्रमशः हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख और अन्य सभी धर्मों की जातियां और जनजातियां शामिल हैं।
भारत के संविधान में एससी, एसटी के हितों की रक्षा के लिए कई प्रावधान हैं। जैसे अस्पृश्यता का उन्मूलन, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, और हिंदू मंदिरों तक पहुंच सुनिश्चित करना, इत्यादि। जमींदारों या सवर्ण लोगों द्वारा अक्सर अनुसूचित जातियों के लोगों से बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था।
जाति व्यवस्था ने शिक्षा और आर्थिक क्षेत्रों में वर्ण-व्यवस्था में ऊपर मौजूद तीन जातियों का एकाधिकार स्थापित कर दिया था। इसलिए संविधान में संसद और विधानसभाओं में कुछ सीटें एससी, एसटी के लिए आरक्षित की गईं। इन समूहों को हिंसा और भेदभाव से बचाने के लिए विशेष कानून और उपाय भी किए गए। जातिगत भेदभाव के मामलों की त्वरित सुनवाई और पीड़ितों को मुआवजा तथा सहायता प्रदान करने के लिए विशेष अदालतें स्थापित की गई हैं।
कानून में निचली जातियों की सुरक्षा के लिए कई सुरक्षा उपाय किए गए हैं। जैसे, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। अनुसूचित जातियों को अक्सर उच्च जातियों के लोगों द्वारा बंधुआ मजदूरी के लिए मजबूर किया जाता था। इसे अब गुलामी का एक रूप माना जाता है।
उच्च जाति के ‘गरीब’ लोगों (ईडब्ल्यूएस) के लिए आरक्षण: वर्ष 2019 में भारत सरकार ने संविधान में संशोधन करके आर्थिक पिछड़ेपन की अवधारणा को लागू किया। ऐसा करके उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को सकारात्मक कार्रवाई और आरक्षण का लाभ दिया गया। इस नए वर्गीकरण को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कहा गया। इसमें उच्च जाति के ‘गरीब’ लोग शामिल हैं। आलोचकों का कहना है कि ये लोग आधिकारिक गरीबी दर से लगभग चार गुना ज्यादा कमाते हैं। उनके लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा के 10 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं।
पत्रकार क्या जांच करें
भारत के संविधान में आरक्षण के माध्यम से निम्न और मध्यम जातियों के लिए कुछ लाभ और संरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके बावजूद कई प्रकार की असमानता कायम है। पत्रकार कई विषयों की जांच करके महत्वपूर्ण स्टोरीज कर सकते हैं। जैसे-
सरकारी नौकरियों की विविधता: सरकारी एजेंसियों को तीन आरक्षित वर्गों के न्यूनतम 49.5 प्रतिशत लोगों को नियुक्त करना आवश्यक है। इस प्रावधान के बावजूद सरकारी एजेंसियों में उच्च जातियों का वर्चस्व देखने को मिलता है। पत्रकारों को इस बात की जांच करनी चाहिए कि इनमें नियुक्तियां कैसे की जाती हैं।
जातिगत हिंसा: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर होने वाले अत्याचार रोकने के लिए भारत में विशेष कानून बनाए गए हैं। इसके बावजूद हर साल इन समुदायों के खिलाफ जातिगत हिंसा के 50,000 से ज़्यादा मामले दर्ज होते हैं। पत्रकार इस बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं कि ऐसी हिंसा किस तरह और क्यों होती है? अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है? क्या पीड़ितों को मुआवज़ा मिलता है?
एससी-एसटी का विकास: प्रत्येक सरकारी मंत्रालय और विभाग को अपने कुल व्यय का 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए और 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए खर्च करना आवश्यक है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, विद्युतीकरण, सड़क संपर्क और मोबाइल/इंटरनेट कनेक्टिविटी, स्वच्छ जल तक पहुँच, व्यावसायिक विकास आदि के विकास संबंधी कार्य प्रमुख हैं। पत्रकारों को यह देखना चाहिए कि क्या ये आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं? एससी-एसटी की आबादी पर इन विकास कार्यों का क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

एससी-एसटी समुदाय के लिए सरकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की मांग को लेकर वर्ष 2020 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बाहर प्रदर्शन। इमेज: शटरस्टॉक।
जनजातीय गांवों का सामाजिक-आर्थिक विकास: संघीय सरकार ने 36,400 से अधिक आदिवासी गांवों के विकास का आदेश दिया है। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार, आवास, सड़क संपर्क आदि पर ध्यान केंद्रित करना है। पत्रकार इन आदेशों की प्रगति की जांच पर आधारित खबरें कर सकते हैं।
दलित गांवों का सामाजिक-आर्थिक विकास: जाति व्यवस्था ने अनुसूचित जातियों को बंजर भूमि में बसने के लिए मजबूर किया है। अपने संवैधानिक दायित्व के तहत केंद्र सरकार 40 प्रतिशत से अधिक एससी आबादी वाले गावों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए एक विकास योजना चलाती है। इस योजना में 11,500 दलित गांवों का बुनियादी ढांचा विकसित करना, कौशल विकास और एससी छात्रों के लिए विशेष शिक्षण शामिल है। इस योजना का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और निगरानी स्थानीय स्वशासन इकाइयों के जिम्मे है। लेकिन इस योजना का ऑडिट शायद ही कभी किया जाता है।
निम्न जातियों के लिए आवासीय विद्यालय: एससी-एसटी बच्चों को अक्सर नियमित स्कूलों में भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए सरकार उनके लिए आवासीय विद्यालय बनाती है। पत्रकार यह पता लगा सकते हैं कि क्या निम्न जाति के बच्चों की इन स्कूलों तक पहुंच है? उनकी स्कूल छोड़ने की दर क्या है? उच्च शिक्षा प्राप्त करने की उनकी क्षमता क्या है?
ओबीसी, एससी, एसटी छात्रों के लिए वित्तीय सहायता: संविधान के अनुसार भारत सरकार को इन वर्गों की प्राथमिक और उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना आवश्यक है। वास्तविक लाभार्थियों तक यह धनराशि पहुंचती है या नहीं, इस बारे में कोई पारदर्शिता नहीं है। पत्रकार इन योजनाओं की जांच करें। पता लगाएं कि ऐसी योजनाएं किस हद तक कारगर हैं।
हाथ से मैला ढोने वालों का पुनर्वास: सफाई का काम करने वालों को सफाई कर्मचारी कहा जाता है। पारंपरिक रूप से भारत में यह केवल दलितों का जाति-आधारित पेशा था। संविधान अब समान अवसर प्रदान करता है। इसके बावजूद सफाई के काम में अन्य जातियों की तुलना में दलितों की संख्या अधिक है। पत्रकार इसकी वजह जान सकते हैं।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC) (NSKFDC)- यह सरकार द्वारा संचालित संस्था है। यह एससी सफाई कर्मचारियों को ब्याज मुक्त ऋण देकर मदद करता है। एजेंसी द्वारा अप्रैल 2018 में किए गए अंतिम सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में लगभग 58,000 से ज़्यादा हाथ से मैला ढोने वाले कर्मचारी हैं। यह लोग अपने नंगे हाथों से पानी रहित शौचालयों की सफाई करते हैं। इन कर्मचारियों की स्थिति और सरकार द्वारा उन्हें अन्य कार्यों के लिए प्रशिक्षित न किए जाने पर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं।

भारत के पानीपत में एक अछूत महिला द्वारा हाथ से मानव मल इकट्ठा करते हुए वर्ष 2010 की फ़ोटो। इस प्रथा पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फिर भी कई राज्यों में यह जारी है। इमेज: शटरस्टॉक
जाति से जुड़ी खबरें कैसे करें?
किसी समूह या व्यक्ति की जाति को जानने से आप उन्हें प्राप्त विशेषाधिकारों को समझने में मदद मिल सकती है। उन्हें किन बाधाओं का सामना करना पड़ा होगा, इसका अनुमान लगाना भी संभव होगा। आज उनके विचारों को किस चीज़ ने आकार दिया है, यह भी समझ पाना आपके लिए संभव होगा।
राजनीति
जाति व्यवस्था को समझे बिना भारत में अच्छी राजनीतिक रिपोर्टिंग करना असंभव है। अधिकांश पार्टियों में एससी और ओबीसी के लिए अलग प्रकोष्ठ हैं। यह वर्ग भारत में बहुसंख्यक आबादी का गठन करता है। इसलिए उनके अलग-अलग प्रकोष्ठ अपनी जाति के मतदाताओं को लुभाने का काम करते हैं। भले ही पार्टियों के पारंपरिक मतदाता उच्च जातियों से हों। उदाहरण देखें।
ओडिशा में ब्राह्मण-कायस्थ आधिपत्य ने राजनीतिक सामाजिक न्याय को पीछे छोड़ दिया। यह स्टोरी जाति के माध्यम से राजनीति का विश्लेषण करती है। यह बताती है कि ओडिशा की राजनीति पर दो उच्च जातियों ने कैसे दशकों तक अपना दबदबा बनाए रखा। जाति-उत्पीड़ित समुदायों को कभी सहायता नहीं मिली। जबकि जनसंख्या में उनका हिस्सा लगभग 40 प्रतिशत है।
किसी व्यक्ति या समुदाय की जाति जानने से उनकी राजनीतिक संबद्धता का अनुमान लगाने में भी मदद मिल सकती है। उच्च जाति के उदारवादी या मध्यमार्गी हिंदू का कांग्रेस समर्थक होने की संभावना अधिक होगी। उच्च जाति के रूढ़िवादी या दक्षिणपंथी हिंदू लोग प्राय: भारतीय जनता पार्टी के मतदाता होंगे। हिंदी पट्टी के अधिक संपन्न ओबीसी लोग समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता पार्टी, या जनता दल यूनाइटेड जैसी समाजवादी पार्टियों में से किसी एक के मतदाता होंगे।
सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डवलपिंग सोसाइटीज- यह मतदाताओं संबंधी डेटा के लिए एक बेहतरीन स्रोत है। इसके अनुसार उच्च जाति के हिंदू आज़ादी के बाद से ही भाजपा के समर्थक रहे हैं। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में दलितों का समर्थन बहुजन समाज पार्टी को मिलता है। मध्यम जाति के खेती-किसानी से जुड़े यादव, उत्तर प्रदेश और बिहार में समाजवादी दलों का समर्थन करते हैं।
जातिगत हिंसा
जाति आधारित हिंसा में आमतौर पर हमलावर सवर्ण हिंदू होते हैं। पीड़ित अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से होते हैं। भारतीय मीडिया आम तौर पर पीड़ितों की जाति बताता है, लेकिन हमलावरों की जाति छिपाता है। हमलावरों के लिए ‘दबंग’ शब्द का इस्तेमाल होता है। हमलावर की जाति का पता नहीं चल पाता है। स्थानीय समाचार संगठनों में उच्च जाति के पत्रकारों की संख्या ज़्यादा है। इसके कारण एससी-एसटी पर होने वाली जातिगत हिंसा के कवरेज में एक अंतर्निहित जातिगत पूर्वाग्रह काम करता है। कुछ मीडिया संस्थान तो हिंसा को उचित ठहराने के लिए असत्यापित खातों के पोस्ट को भी प्रकाशित करते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जाति-आधारित हिंसा की कवरेज अक्सर हमलावरों के नज़रिए से की जाती है।
जाति-आधारित हिंसा पर एक निष्पक्ष और ठोस रिपोर्ट में हमलावरों की जातिगत पहचान उजागर होनी चाहिए। हिंसा की जाँच होनी चाहिए। पीड़ितों को वास्तविक लोगों के रूप में चित्रित किया जाना चाहिए, न कि केवल निचली जाति के सदस्यों के रूप में। उन्हें मानवीय संवेदना से रहित असहाय या शक्तिहीन व्यक्ति के रूप में चित्रित नहीं करना चाहिए। उनकी अपनी आवाज़ को भी उजागर करना चाहिए, ताकि उनकी गरिमा और शक्ति का सम्मान हो। जब मामला अदालत में पहुंचे, तो यह जांच करनी चाहिए कि अदालत के फैसले में जातिगत पूर्वाग्रह है अथवा नहीं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष एससी-एसटी के विरुद्ध जातिगत हिंसा के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं।
किसी जाति के व्यक्ति का साक्षात्कार
जाति किसी के रंग, बालों या अन्य शारीरिक विशेषताओं में नहीं दिखाई देती। एक विदेशी व्यक्ति के लिए, किसी भी जाति के व्यक्ति से संपर्क करने का कोई सामाजिक नियम नहीं है। सभी जातियों के लोग पत्रकारों से समान रूप से बातचीत करते हैं। पत्रकार किसी से भी आदर के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन अनुसूचित जाति का कोई पत्रकार यदि किसी सवर्ण रूढ़िवादी हिंदुओं से बात करना चाहे, तो इसके लिए अलग सामाजिक नियम हो सकते हैं। हिंदू जाति व्यवस्था में अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों को अपवित्र माना जाता है। इसलिए उनके द्वारा पूछताछ किए जाने पर उच्च जाति का व्यक्ति बुरा मान सकता है। अनुसूचित जाति के पत्रकारों को हिंदू मंदिरों की रिपोर्टिंग करते समय भी सावधानी बरतनी चाहिए। ऐतिहासिक रूप से हिंदू मंदिरों में अनुसूचित जातियों के प्रवेश पर प्रतिबंध था। भारत में कुछ मंदिरों में यह प्रतिबंध अभी भी लागू है।
जनजातियों पर रिपोर्टिंग करते समय, याद रखें कि भारत में केवल कुछ पहाड़ी जनजातियों के पास ही अपने लोगों की ओर से बोलने के लिए आदिवासी नेता होते हैं। हालांकि किसी भी जनजाति के किसी भी व्यक्ति से संपर्क करने पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं हैं।

इमेज: सिद्धेश गौतम, जीआइजेएन
आंकड़े और संसाधन
जाति संबंधी आंकड़े
जातियों की गणना केवल अंग्रेज़ी शासकों द्वारा की जाती थी। वे जाति को भारतीय समाज की नींव और सामाजिक स्तर में बदलाव को मापने का एक महत्वपूर्ण साधन मानते थे। ब्रिटिश शासन के तहत, जनगणना विभाग हर दस साल में जाति, नस्ल और जनजाति के आधार पर भारतीय जनसंख्या की गणना और वर्गीकरण करता था। आज भी किसी समुदाय को कानूनी लाभ मिलने संबंधी विवाद के मामले में शिक्षाविद और वकील अंग्रेजों की उन रिपोर्टों का हवाला देते हैं।
जातियों के संबंध में अंग्रेजों की जनगणना रिपोर्टों का काफी उपयोग है। इनमें व्यापक नृवंशविज्ञान और मानवशास्त्रीय विश्लेषण मिलता है। यह बीसवीं सदी के शुरुआती वर्षों और ब्रिटिश शासन काल की हैं। यहाँ अलग-अलग वर्षों की रिपोर्ट के लिंक दिए गए हैं – 1901, 1911 और 1931।
स्वतंत्रता के बाद
कुछ विश्लेषकों का मानना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में कभी भी सभी जातियों की जनगणना नहीं हुई है। कारण यह, कि भारतीय शासक वर्ग में मुख्यतः उच्च जातियों का वर्चस्व है। जातियों की जनगणना से राजनीतिक क्षेत्र पर उच्च जातियों के एकाधिकार का पर्दाफ़ाश हो जाएगा। गृह मंत्रालय के अधीन भारतीय जनगणना कार्यालय बनाया गया है। यह पूरी जनसंख्या की गणना करता है। लेकिन इसमें केवल यह पूछा जाता है कि क्या आप संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त दो संरक्षित समूहों, अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं।
अनुसूचित जातियों के रूप में सूचीबद्ध जातियों की राज्यवार संख्या यहां उपलब्ध है। पहली बार यह सूची 1936 में ब्रिटिश शासन के दौरान बनी थी। तब से इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है।
स्वतंत्रता के बाद से जातिगत जनगणना का एकमात्र प्रयास 2010 में हुआ। एससी तथा ओबीसी दलों के समर्थन से बनी यूपीए सरकार ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में गरीबी दर निर्धारित करने हेतु देश भर में जातियों की गणना कराई। जनगणना में एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण किया गया। इसमें घरेलू आय, भूमि स्वामित्व और सरकारी नौकरियों जैसी जानकारी शामिल थी। लेकिन सरकार ने इन जातिगत आंकड़ों को जारी नहीं किया। केवल एससी और एसटी के संबंध में सर्वेक्षण का एक हिस्सा जारी किया गया। यह आज भी एक महत्वपूर्ण डेटासेट है। इसे सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना (SECC) कहा जाता है। इसमें आय वितरण, आवास के प्रकार, रोज़गार के स्रोत, संपत्ति के स्वामित्व और सामाजिक कमज़ोरियों सहित विभिन्न मानदंडों का उपयोग करके ग्रामीण एएसी और एसटी परिवारों संबंधी विस्तृत आंकड़े उपलब्ध हैं।
भारत के 28 राज्यों में से बिहार पहला और एकमात्र राज्य है जिसने 2023 में जातिगत जनगणना करके आंकड़े जारी किए। सर्वेक्षण में आय, शिक्षा, आवास और नौकरियों में असमानताएँ सामने आईं। यह उजागर हुआ कि कैसे उच्च जातियों के पास जनसंख्या के अपने हिस्से की तुलना में संसाधनों का अत्यधिक हिस्सा है।
सरकारी नौकरियों में आरक्षण का आंकड़ा
कानून के अनुसार, सभी सरकारी नौकरियों में एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और ओबीसी के लिए 27% सीटें आरक्षित हैं। लेकिन यह पता करना मुश्किल है कि क्या वास्तव में ऐसा होता है। सरकार प्राय: स्वेच्छा से इसके आंकड़े जारी नहीं करती। फिर भी, एससी और एसटी के कल्याण पर संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्टों में कुछ आंकड़े मौजूद हैं। इनसे सरकारी विभागों के भीतर विविधता की जांच करना संभव है। यहां विविधता का अभिप्राय इन नौकरियों में व्यापक आबादी का प्रतिनिधित्व होने से है।
सरकारी विश्वविद्यालयों, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, चिकित्सा संस्थानों और सरकारी स्कूलों में विविधता (reports on diversity ) पर आधिकारिक रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। इसके अलावा, भारत की संघीय एजेंसियों ( diversity in India’s federal agencies) और वित्तीय संस्थानों (financial institutions.) में विविधता पर सर्वेक्षण भी उपलब्ध हैं।
जातिगत हिंसा के आंकड़े
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एक सरकारी एजेंसी है। यह देश भर में होने वाले अपराधों के आंकड़े प्रकाशित करती है। इनमें एससी और एसटी पर हिंसा के मामले भी शामिल हैं।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय – यह जातिगत हिंसा के मामलों में न्याय प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है। ये रिपोर्टें जातिगत हिंसा के मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए गठित विशेष न्यायालयों के कामकाज, इन मामलों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति, पीड़ितों के साथ व्यवहार और ऐसे मामलों की निगरानी के लिए राज्य निगरानी समितियों के संचालन की जांच करती हैं। यह मंत्रालय नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम के कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार करता है। यह कानून अस्पृश्यता खत्म करने और सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है। यह रिपोर्ट जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता को रोकने के लिए बनाए गए संस्थागत तंत्रों के कामकाज की भी जांच करती है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) की वार्षिक रिपोर्टें भी उपलब्ध हैं। यह एक सरकारी निकाय है। यह एससी के संरक्षण और कल्याण की निगरानी करता है। इसमें अनुसूचित जातियों के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और छात्रवृत्ति कोटा कार्यक्रमों में पक्षपात पर रिपोर्टें शामिल हैं।
एससी और एसटी के सामाजिक-आर्थिक विकास पर आंकड़े
निम्न जातियों पर पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध हैं। देश के वार्षिक बजट दस्तावेज़ में आप देख सकते हैं कि एससी तथा अन्य जातियों के लिए राष्ट्रीय व्यय का कितना हिस्सा आवंटित किया गया है। कानून के तहत, संघीय सरकार को क्रमशः एससी के लिए 15 प्रतिशत और एसटी के लिए 7.5 प्रतिशत खर्च करना आवश्यक है।
- विभिन्न परियोजनाओं के लिए वित्तीय आवंटन, साक्षरता दर और सरकार में जातियों के प्रतिनिधित्व सहित अन्य जानकारी से संबंधित डेटा सेट प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के ओपन-डेटा प्लेटफ़ॉर्म पर ‘वेलफेयर ऑफ एससी एसटी’ खोजें। अनुसूचित जातियों के लिए बजट आवंटन को स्पष्ट करने वाले दिशानिर्देश देखें। ये दिशानिर्देश सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए एक आधार प्रदान कर सकते हैं। अन्य संसाधन हैं:
- एससी के कल्याण के लिए बजटीय आवंटन पर डेटा।
- एससी/एसटी के कल्याण की संसदीय समिति।
- अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण और कल्याण की निगरानी करने वाली संस्था, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) की वार्षिक रिपोर्ट।
अतिरिक्त डेटा:
वित्तीय अनुदान के लिए चिन्हित एससी गांवों की राज्यवार सूची है। इन गांवों में सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय संसाधनों के आवंटन और लक्षित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की आवश्यकता है।
किसी प्रखंड या ज़िले में अनुसूचित जाति की आबादी के संकेन्द्रण के आँकड़े उपलब्ध हैं:
- 40 प्रतिशत तक एससी निवासियों वाले प्रखंड।
- 40 से 50 प्रतिशत तक एससी निवासियों वाले प्रखंड।
- 50 प्रतिशत से अधिक एससी निवासियों वाले प्रखंड।
- 40 प्रतिशत से अधिक एससी आबादी वाले जिले।
- केंद्र सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सूची के अनुसार प्रत्येक राज्य में ओबीसी की संख्या। इससे पता चलता है कि कौन से समुदाय किस कोटे और लाभ के पात्र हैं।
- वर्ष 2011 में हुई जनगणना के आधार पर एससी की साक्षरता दर।
- वर्ष 2004-2005 में एससी तथा ओबीसी में बीपीएल आबादी का राज्यवार प्रतिशत।
- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की वार्षिक रिपोर्टें– यह शैक्षणिक संस्थानों, सार्वजनिक एजेंसियों, वित्तीय संस्थानों और कल्याणकारी पहलों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के प्रतिनिधित्व के आंकड़े प्रदान करती हैं।
- हाथ से मैला ढोने वालों संबंधी निम्नलिखित आंकड़े उपलब्ध हैं।
जाति व्यवस्था पर सबसे व्यापक शोध बीसवीं सदी के आरंभ में किया गया था। ब्रिटिश मानवविज्ञानियों और नृवंशविज्ञानियों ने प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए भारत की विविध जनसंख्या को समझने का प्रयास किया था। तब भारतीय जनसंख्या के वर्गीकरण के लिए नस्ल और जनजाति के साथ जाति को भी एक मानदंड के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उनके वर्गीकरण के आधार पर उस काल की भारत की आधिकारिक जनगणना रिपोर्टों का हिस्सा हैं।
पूर्व न्याय मंत्री डॉ. अंबेडकर ने इस विषय पर भारतीय विद्वानों में सबसे प्रामाणिक दस्तावेज तैयार किए।
जातियों पर काम करने वाले संगठन
ऐसे कई सरकारी और गैर-सरकारी संगठन हैं। ये पत्रकारों के लिए एक बेहतरीन स्रोत हो सकते हैं।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) – यह एक सरकारी निकाय है। इसका काम अनुसूचित जातियों को शोषण से बचाना और उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हितों को बढ़ावा देना है। एनसीएससी की वेबसाइट पर यह कुछ सेक्शन महत्वपूर्ण हैं –
- वार्षिक रिपोर्ट्स।
- विशेष रिपोर्ट्स।
- सुनवाई के कार्यवृत्त।
- आयोग की बैठक।
- एससी पर केंद्रित नीतियों और कानूनों की निगरानी और कार्यान्वयन।
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) – यह अनुसूचित जनजातियों को शोषण से बचाता है और उनके हितों को बढ़ावा देता है। इसकी वेबसाइट पर इस समूह के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों, अनुसूचित जनजातियों के लिए संघीय सरकार की विकास नीतियों, शिकायत सुनवाई, अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अत्याचारों के विश्लेषण और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर प्रशासनिक और विधायी समीक्षाओं की जानकारी उपलब्ध है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (एनसीबीसी) – अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों की रक्षा के लिए एक सार्वजनिक निकाय। यह सरकारी नीति और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन से संबंधित डेटा तक पहुँचने के लिए एक बेहतरीन संसाधन है।
राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (एनसीएसके) – हाथ से मैला ढोने वालों और सफाई कर्मचारियों (सेप्टिक टैंक और सीवर साफ़ करने वाले) के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए गठित एक सरकारी निकाय। इसकी वार्षिक रिपोर्टें बताती हैं कि इनमें से कितने लोग काम के दौरान मारे जाते हैं। उनके अधिकारों की रक्षा करने वाले कानूनों के क्रियान्वयन की जानकारी भी मिलती है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय – यह निचली जातियों के हितों की रक्षा करने वाले कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कार्य करता है। वेबसाइट में बेहतरीन आंकड़े मिल जाएंगे।
जनजातीय कार्य मंत्रालय – यह आदिवासियों संबंधी कार्यक्रमों और कानूनों की निगरानी करता है। वेबसाइट अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक, आवास और रोज़गार कार्यक्रमों पर आँकड़े प्रदान करती है।
अंतर्राष्ट्रीय दलित एकजुटता नेटवर्क (आईडीएसएन) – यह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, विकास एजेंसियों और दलित एकजुटता समूहों का एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है। इसका उद्देश्य दलित मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना है। आईडीएसएन जाति व्यवस्था पर किए जा रहे समकालीन अध्ययनों का एक बड़ा स्रोत है।
दलित मानवाधिकारों पर राष्ट्रीय अभियान (एनसीडीएचआर) – यह मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों का मंच है। यह जाति पर निरंतर अध्ययन प्रकाशित करता है। यह अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए सरकारी बजट आवंटन का भी विश्लेषण करता है।
क्या करें और क्या न करें
- जातिगत पहचान बताना किसी तथाकथित निम्न पदस्थ व्यक्ति के लिए संकोच का विषय होता है। विशेष रूप से अनुसूचित जाति के सदस्यों के लिए यह शर्मनाक है। उनकी जाति की पहचान के कारण कार्यस्थल भेदभाव हो सकता है। कोई मकान मालिक उन्हें किराए पर घर देने से मना कर सकता है। इसलिए किसी पत्रकार को अपनी कहानी में किसी एससी व्यक्ति की जाति तभी बतानी चाहिए, जब वह इसके लिए सहमत हो।
- भारतीय उपनाम जातिगत मूल को दर्शाते हैं। लेकिन ये सभी जातियों में एक समान नहीं हैं। निम्न जाति के सदस्य अक्सर अपनी जाति छिपाने और उच्च जाति के उपनामों का उपयोग करते हैं। किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख करने से पहले उसका जाति नाम पूछना हमेशा उचित होता है।
- पत्रकारों को जातिगत हिंसा या भेदभाव के मामलों का विश्लेषण करते समय विभिन्न जाति समुदायों के बीच संबंधों, एक-दूसरे पर आर्थिक निर्भरता और भूमि स्वामित्व के पैटर्न को समझने का प्रयास करना चाहिए।
- सांप्रदायिक हिंसा पर रिपोर्टिंग करते समय अपराधियों की जाति का उल्लेख करना महत्वपूर्ण है। जैसे, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हिंसा का मामला। अगर इसमें जाति का ज़िक्र नहीं होता, तो यह हिंदुओं की एकरूप पहचान को बढ़ावा देता है, जो कि सच नहीं है। इससे निचली जातियों के हिंदुओं के ख़िलाफ़ उच्च जातियों के हिंदुओं के हितों को भी बढ़ावा मिलता है।
- जाति व्यवस्था धन, शिक्षा और राजनीतिक सत्ता के मामले में शीर्ष तीन वर्गों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को लाभ पहुँचाती है। निचली जातियों के नुकसानों पर चर्चा करते समय इसका ज़िक्र होना चाहिए।
केस स्टडीज़
अलगाव से लेकर श्रम तक: जेल में भी लागू है मनुवादी व्यवस्था – द वायर इंडिया ने इस स्टोरी में भारत की जेलों में जातिगत भेदभाव की गहरी पड़ताल की है। बताया है कि कैदियों के अनुभव उनके आर्थिक आधार के साथ ही उनकी जाति के आधार पर भी भिन्न थे। जेल के संचालन को नियंत्रित करने वाली जेल नियमावली में भी यह भेदभाव शामिल है। एक दलित कैदी को शौचालय और सीवर साफ़ करने के लिए नियुक्त किया जाता है। उच्च वर्ग के कैदियों को आमतौर पर खाना पकाने जैसे काम मिलते हैं।
उत्तराखंड: एक सवर्ण राज्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है – राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लंबे आंदोलन के बाद भारत में उत्तराखंड का एक अलग राज्य बना। इस लेख में पत्रकार महेश सी. डोनिया ने जातिगत विभाजन के परिप्रेक्ष्य से राज्य के निर्माण पर पुनर्विचार किया है। बताया है कि अपने गठन के समय से ही यह अनुसूचित जातियों, विशेष रूप से दलित आबादी के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को बढ़ावा देने पर आधारित है। ऐसा करने वालों को कोई दंड नहीं दिया गया। अधिकारियों ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया।
अतिरिक्त संसाधन
भारतीय मीडिया संगठनों में उत्पीड़ित समुदायों की अनुपस्थिति के कारण जाति पर बहुत कम पत्रकारिता होती है। जो लोग इस विषय पर गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए नीचे कुछ संसाधन दिए गए हैं:
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित अंबेडकर की संकलित रचनाएं, उनके निबंध व भाषण महत्वपूर्ण हैं। खासकर इन दोनों का अध्ययन आपके लिए उपयोगी होगा:
संसद की एक रिपोर्ट: इसमें भारतीय न्यायपालिका में जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद होने की एक दुर्लभ आधिकारिक स्वीकारोक्ति है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी, जो न्यायाधीशों की नियुक्तियों में सकारात्मक कार्रवाई का प्रयोग नहीं करता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि न्यायपालिका में विविधता की कमी है। उच्च जाति के हिंदू न्यायाधीश अक्सर जातिगत पूर्वाग्रह के साथ आपराधिक मामलों का फैसला करते हैं। मुकदमों का परिणाम अक्सर अनुसूचित जाति के लोगों को सजा देने और उच्च जाति के अभियुक्तों को दोषमुक्त करने के रूप में सामने आता है।
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की रिपोर्ट: यह न्यायपालिका के भीतर मौजूद जातिगत पूर्वाग्रह को उजागर करने वाला एक और आधिकारिक दस्तावेज है। इस दस्तावेज में न्यायिक प्रणाली में विविधता की कमी का पता चलता है। इसमें अनुसूचित जाति के पीड़ितों के साथ भेदभाव और उच्च जाति के न्यायाधीशों के बीच जातिगत पूर्वाग्रह के तथ्य शामिल हैं।
मिट्टी के घरों से विद्रोही – दलित और बिहार में माओवादी क्रांति: जॉर्ज जे. कुन्नथ की यह पुस्तक बताती है कि कैसे जाति व्यवस्था आज भी दलितों के विरुद्ध हिंसा को बढ़ावा देती है। जातिगत हिंसा से अपने समुदाय की रक्षा के लिए दलितों ने हथियारबंद होना क्यों शुरू किया? यह पुस्तक 1990 के दशक में दलितों की स्थिति का विश्लेषण करती है, जब उच्च जाति के लोगों ने दलित समुदाय के विरुद्ध नरसंहारों की योजना बनाई थी।
GIJN टीम द्वारा संपादित : निकोलिया अपोस्टोलू, रीड रिचर्डसन, दीपक तिवारी और अमेल गनी।
 सागर चौधरी कारवां में स्टाफ राइटर हैं। वह राजनीति, शासन, समाज, धर्म और जाति पर लंबी खबरें और आलेख लिखते हैं। वह बिहार में रहते हैं। मध्य, उत्तरी और पूर्वी भारत के दूरदराज के इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें शेवनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप 2024 और एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप 2023 प्राप्त हो चुकी है। उन्हें 2019 और 2020 में रेड-इंक पत्रकारिता पुरस्कार भी मिला। भारत और फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी विमान सौदे पर उनकी स्टोरी का उपयोग एक जनहित याचिका में तथ्य की पुष्टि के लिए किया गया। वह 14 वर्षों से पत्रकार हैं। प्रारंभ में उन्होंने एक क्षेत्रीय दैनिक में अपराध रिपोर्टर और एक सामुदायिक रिपोर्टर के रूप में काम किया।
सागर चौधरी कारवां में स्टाफ राइटर हैं। वह राजनीति, शासन, समाज, धर्म और जाति पर लंबी खबरें और आलेख लिखते हैं। वह बिहार में रहते हैं। मध्य, उत्तरी और पूर्वी भारत के दूरदराज के इलाकों से रिपोर्टिंग करते हैं। उन्हें शेवनिंग साउथ एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप 2024 और एशिया जर्नलिज्म फेलोशिप 2023 प्राप्त हो चुकी है। उन्हें 2019 और 2020 में रेड-इंक पत्रकारिता पुरस्कार भी मिला। भारत और फ्रांस के बीच अंतर-सरकारी विमान सौदे पर उनकी स्टोरी का उपयोग एक जनहित याचिका में तथ्य की पुष्टि के लिए किया गया। वह 14 वर्षों से पत्रकार हैं। प्रारंभ में उन्होंने एक क्षेत्रीय दैनिक में अपराध रिपोर्टर और एक सामुदायिक रिपोर्टर के रूप में काम किया।
अनुवाद: डॉ. विष्णु राजगढ़िया